भारत में नदी जोड़ परियोजना: लाभ और पर्यावरणीय चुनौतियाँ
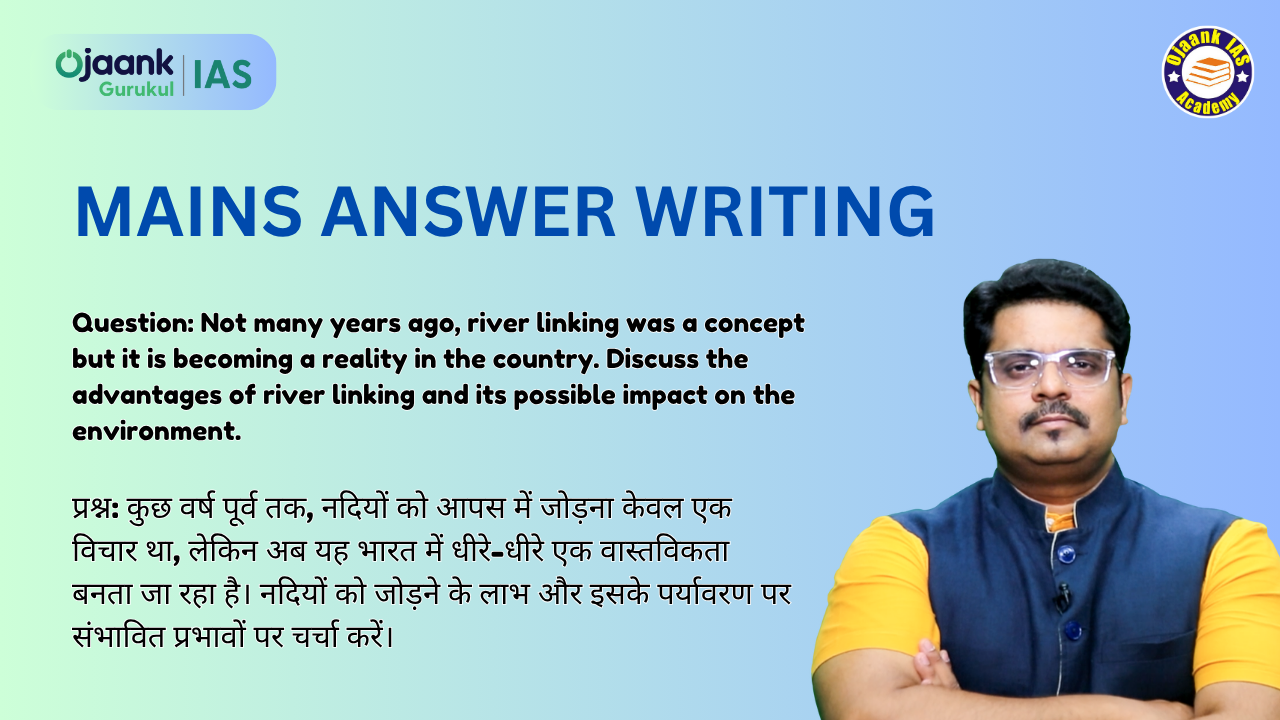
प्रश्न: कुछ वर्ष पूर्व तक, नदियों को आपस में जोड़ना केवल एक विचार था, लेकिन अब यह भारत में धीरे-धीरे एक वास्तविकता बनता जा रहा है। नदियों को जोड़ने के लाभ और इसके पर्यावरण पर संभावित प्रभावों पर चर्चा करें।
उत्तर:
पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन ने भारत को नदी जोड़ने की अवधारणा को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है। हाल ही में पोलावरम या पट्टीसीमा परियोजना में गोदावरी को कृष्णा नदी से जोड़ने की व्यवस्था की गई, जिससे कृष्णा को जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। लेकिन यदि इस तरह की परियोजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए, तो इसके लाभों के साथ-साथ पर्यावरण पर संभावित प्रभावों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना आवश्यक है।
नदी जोड़ने की परिभाषा:
नदी जोड़ने का अर्थ है देश की विभिन्न नदियों को नहरों और जलाशयों के नेटवर्क के माध्यम से आपस में जोड़ना। इस संबंध में कई अध्ययन किए गए हैं जो इसके लाभों और पर्यावरणीय प्रभावों को दर्शाते हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण अध्ययन नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी (National Water Development Agency) द्वारा किया गया है। इन अध्ययनों के आलोक में इसके लाभ और प्रभाव को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है:
नदी जोड़ने के लाभ:
-
भारत मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है। लगभग 70% या उससे अधिक वर्षा जुलाई से सितंबर के बीच तीन महीनों में होती है। यह वर्षा भी समान रूप से नहीं होती। यही कारण है कि भारत बाढ़ और सूखे दोनों की समस्या से एक साथ जूझता है—कई बार देश के विभिन्न हिस्सों में एक ही समय में।
नदी जोड़ना इस समस्या का समाधान माना जाता है, जिसके तहत अधिक जल वाले क्षेत्रों से जल की आपूर्ति जल-अभाव वाले क्षेत्रों में की जाएगी।
-
इससे जल उपयोग दक्षता (water use efficiency) में वृद्धि होगी।
-
यह बाढ़ की रोकथाम और नियंत्रण में सहायक हो सकता है।
-
यह सूखे की स्थिति को कम कर सकता है।
-
यह शुष्क, अर्ध-शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल उपलब्ध करा सकता है, जिससे वहाँ नए भूमि क्षेत्रों को सिंचित कृषि के दायरे में लाया जा सकता है और उत्पादन कई गुना बढ़ सकता है।
-
यह भूजल और जलाशयों को रिचार्ज कर सकता है और नए जलाशयों का निर्माण भी संभव होगा।
-
नदी जोड़ने के माध्यम से एक व्यापक रूप से जुड़ा जलमार्ग तंत्र विकसित किया जा सकता है, जो माल-परिवहन के लिए अधिक पर्यावरण-सुलभ और लागत-कुशल माध्यम हो सकता है।
पर्यावरण पर संभावित प्रभाव:
[A] सकारात्मक प्रभाव:
-
जलमार्ग आधारित परिवहन अधिक पर्यावरण के अनुकूल होता है और इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आ सकती है।
-
इससे जल-विद्युत उत्पादन की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं, जो पर्यावरण के लिए लाभदायक ऊर्जा स्रोत है।
-
जल की आपूर्ति शुष्क क्षेत्रों में हरियाली और वनों के विकास को बढ़ावा दे सकती है।
[B] नकारात्मक प्रभाव:
-
नदी जोड़ परियोजनाओं के लिए कई वनों की कटाई आवश्यक हो सकती है।
-
यह जैव विविधता हॉटस्पॉट्स और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर सकता है।
-
यह अब तक असंबद्ध पारिस्थितिक क्षेत्रों को नदियों और जल चैनलों से जोड़ देगा। इससे कई पौधों और जानवरों की प्रजातियाँ नए क्षेत्रों में पहुँच सकती हैं, जिनमें कुछ आक्रामक प्रजातियाँ भी हो सकती हैं।
-
शुष्क क्षेत्रों में अधिक जल की आपूर्ति मिट्टी और स्थलाकृति के लिए अनुपयुक्त हो सकती है, जिससे मिट्टी में लवणता (salinity) की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
-
नहरों के किनारे की मिट्टी में भी लवणता बढ़ सकती है।
-
जल प्रवाह में बदलाव से नदियों के मार्ग में परिवर्तन का खतरा हो सकता है, जो पारिस्थितिक आपदा का कारण बन सकता है।
-
जल प्रवाह, बाढ़ और सूखे के स्वरूप में परिवर्तन उन प्रजातियों के लिए खतरा बन सकता है जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित हैं।
-
जलाशयों का निर्माण बाढ़ और जलभराव के माध्यम से क्षेत्रों को डुबो सकता है। जैसे कि प्रस्तावित केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना पन्ना टाइगर रिज़र्व के बड़े हिस्से को डुबो सकती है।
निष्कर्ष:
इन लाभों और प्रभावों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि एक बहुत ही विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (Environmental Impact Assessment) किया जाना चाहिए। केवल सावधानीपूर्वक लागत-लाभ विश्लेषण (Cost-Benefit Analysis) के बाद ही बड़े स्तर पर नदी जोड़ परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
तब तक जल संरक्षण और वर्षा जल संग्रहण (Rainwater Harvesting) के माध्यम से जल संकट से निपटना चाहिए।
-1753796137357.jpeg)